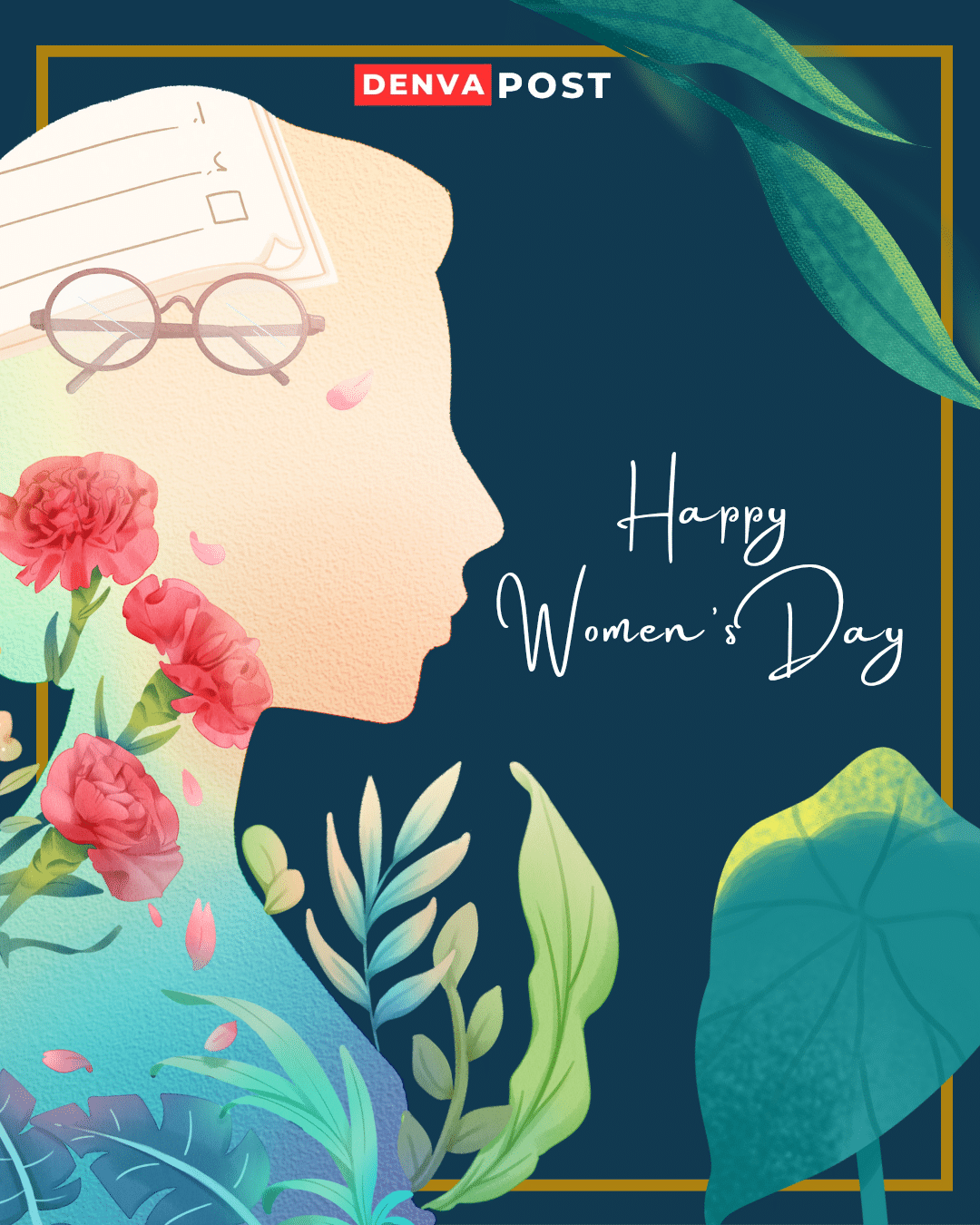भारतीय संविधान किसी अमूर्त आदर्श पर नहीं, बल्कि गणनीय नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित है। “हम, भारत के लोग” की उद्घोषणा तभी अर्थवान होती है, जब राज्य यह स्वीकार करे कि हर नागरिक को गिना जाना, पहचाना जाना और प्रतिनिधित्व मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है। एक दशक से राष्ट्रीय जनगणना का न होना इसी संवैधानिक स्वीकृति से पीछे हटने का संकेत है।
जनगणना: केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, संवैधानिक आवश्यकता
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 यह स्पष्ट करते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं की संरचना जनसंख्या के आधार पर तय होगी। परिसीमन, प्रतिनिधित्व का अनुपात और “एक व्यक्ति, एक मत” का सिद्धांत—all जनगणना पर निर्भर हैं। जब जनगणना नहीं होती, तब प्रतिनिधित्व अनुमान पर आधारित हो जाता है, न कि तथ्य पर। यह संविधान की आत्मा के विपरीत है।
इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15, 16 और 38 के तहत समानता और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, वह भी जनसांख्यिकीय आंकड़ों के बिना खोखली हो जाती है। कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण, आरक्षण नीति की समीक्षा और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण—सब जनगणना के अभाव में संवैधानिक दावों से अधिक राजनीतिक वक्तव्य बनकर रह जाते हैं।
मताधिकार और जनगणना का संवैधानिक संबंध
मतदान का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के अनुसार यह लोकतांत्रिक संरचना का अनिवार्य अंग है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार की सुरक्षा तभी संभव है, जब मतदाता सूची का आधार सत्यापित और अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों पर टिका हो।
जनगणना के बिना संचालित एसआईआर (Special Intensive Revision) जैसी प्रक्रियाएँ इस संवैधानिक संतुलन को तोड़ देती हैं। जब राज्य के पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस जनसांख्यिकीय आधार नहीं होता कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, तब मतदाता सूची से नाम हटाना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि संवैधानिक जोखिम बन जाता है।
दस्तावेजों की असमान मांग और अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 राज्य को समानता और गैर-मनमानी की बाध्यता देता है। लेकिन व्यवहार में एक विरोधाभास उभरता है—राज्य नागरिकों से नागरिकता और पहचान के दस्तावेज मांगता है, जबकि स्वयं अपनी आबादी का दस्तावेजीकरण (जनगणना) करने से बचता है। यह असमानता केवल नैतिक नहीं, संवैधानिक समस्या है।
जब दस्तावेजों की मांग चयनात्मक हो जाती है और उसका प्रभाव मुख्यतः गरीब, प्रवासी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक नागरिकों पर पड़ता है, तब यह अनुच्छेद 14 और 21 दोनों के उल्लंघन की स्थिति बनाती है। जीवन और गरिमा का अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी तक विस्तारित है।
जवाबदेही का संवैधानिक संकट
संविधान में राज्य की शक्ति को अनुभवजन्य जवाबदेही से जोड़ा गया है। जनगणना इसी जवाबदेही का मूल उपकरण है। इसके अभाव में संप्रभु शक्ति प्रमाण से नहीं, अनुमान से संचालित होने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र को “कानून के शासन” से हटाकर “प्रक्रिया के शासन” में बदल देती है—जहाँ नियम तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे सत्य नहीं होता।
यदि राज्य बिना यह सिद्ध किए कि करोड़ों नागरिक या तो मृत हैं, देश छोड़ चुके हैं या उनकी नागरिकता समाप्त हो चुकी है, उन्हें मतदाता सूची से हटा सकता है, तो यह संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच को निष्प्रभावी कर देता है।
जनगणना का टलना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि संवैधानिक चूक है। यह प्रतिनिधित्व, समानता और मताधिकार—तीनों पर एक साथ आघात करता है। संविधान नागरिकों से निष्ठा की अपेक्षा करता है, लेकिन बदले में राज्य से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी करता है।
जब राज्य नागरिकों को गिनना बंद कर देता है, तब वह संविधान के मूल वादे से पीछे हटता है। और जिस लोकतंत्र में गिने जाने का अधिकार असुरक्षित हो जाए, वहाँ मतदान का अधिकार भी अंततः औपचारिकता भर रह जाता है।